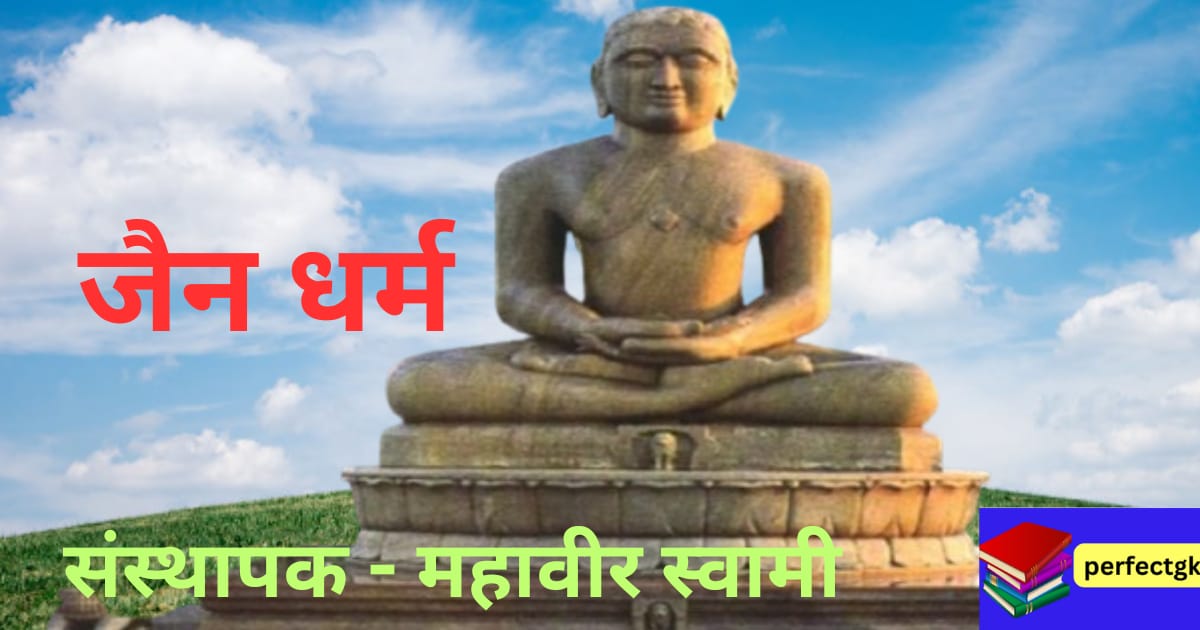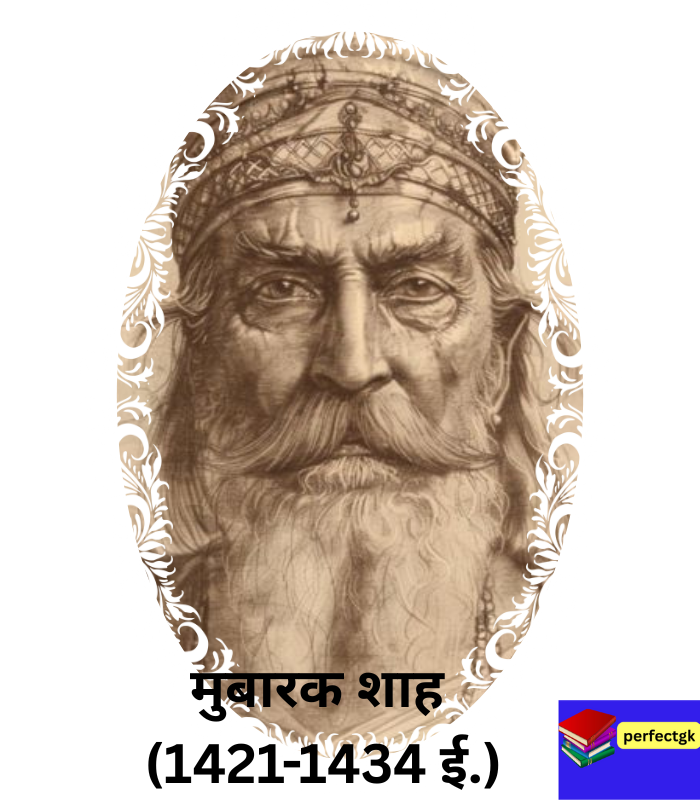छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म उस समय हुआ जब भारत में मुगल सत्ता अपने चरम पर थी। मुगल बादशाह औरंगजेब हिन्दू धर्म को अपनी तलवार की दम पर समाप्त करना चाहता था। इस समय अधिकांश राजे-महाराजे दिल्ली दरबार मे सिजदा कर रहे थे। या अपनी रियासतों की रक्षा के लिए मुगल बादशाह की गुलामी स्वीकार कर चुके थे। इसी समय मात्र 12 वर्ष की उम्र में पिता से प्राप्त पूना की जागीर से छत्रपति शिवाजी महाराज ने माँ जीजाबाई और अपने गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोणदेव की देखरेख/संरक्षण में मुगलों से हिन्दू धर्म की रक्षा करना एक मुख्य उद्देश्य बना लिया था।
और पढ़े :-महात्मा गाँधी (1869-1948) |पुस्तकें|संस्थाये|आन्दोलन |राजनितिक गुरु
छत्रपति शिवाजी का प्रारंभिक जीवन :-
20 अप्रैल 1627 ई0 में शिवाजी का जन्म महाराष्ट्र के पूना के उत्तर दिशा
मे स्थित जुन्नाव नगर के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था ।
शिवाजी जो कि बाद मे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पिता का नाम शाह जी भोसले और माता जीजा बाई थी।
जीजाबाई देवगिरि के यादवराज परिवार के महान जागीर दार यादव राय की पुत्री थी ।
शाह जी भोसले अहमदनगर और बीजापुर के राजनैतिक संघर्ष में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। जिससे यह शक्तिशाली और सम्मानित सामन्त थे ।
शाहजी भोसले द्वारा तुकाबाई मोहिते नामक स्त्री से दूसरी शादी की परिणाम स्वरूप जीजाबाई अपने पुत्रा शिवाजी को लेकर पति से अलग रहने लगी ।
शिवाजी बचपन में ही पिता से अलग हो गए लेकिन पिता भोसले र्ने इनकी देखभाल व शिक्षा के लिए बफादार सेवक दादाजी कोंणदेव को नियुक्त कर दिया था।
शिवाजी को पिता शाह जी भोसलें से 12 वर्ष की उम्र में पूजा की जागीर प्राप्त हुई।
12 वर्ष की अल्पायु में शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर सें कर दिया गया।
शिवाजी पर उनकी माता जीजाबाई का प्रभाव अधिक था वह स्वभाव से बड़ी धार्मिक थी। इसलिए शिवाजी के चरित्र निर्माण मे धार्मिक रुचि पैदा करने हेतु रामायण, महाभारत तथा अन्य प्राचीन काल के हिन्दू वीरो की कहानियां सुनाया करती थी।
माता जीजाबाई द्वारा शिवाजी से हिन्दुओं की तीन परम पवित्र वस्तुओं ब्राह्मण, गौ, और जाति की रक्षा के लिए प्रेरित किया गया।
शिवाजी के जीवन संघर्ष का एक मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। क्योंकि यह किसी मुसलमान शासक के जागीरदार बनकर जीवन व्यतीत करना नही चाहते थे। इस कट्टरता के कारण शिवाजी का मतभेद अपने संरक्षक दादाजी कोणदेव से था।
शिवाजी का मुगल सत्ता को समाप्त करने का उद्देश्य न होकर एक स्वतंक राज्य की स्थापना’ करना था। इसलिए वह मराठी की बिखरी शक्ति को संगठित करके महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र हिन्दू राज्य की स्थापना करना चाहते थे।
छत्रपति शिवाजी के विजय अभियान (conquests):-
1647 ई में शिवाजी के संरक्षक कोंणदेव की मृत्यु के पहले इनके संरक्षण में पूना के आस पास के किलो को जीत लिया गया। हांलाकि इस कार्य से कोंणदेव सहमत नहीं थे।
20 वर्ष की उम्र में छत्रपति शिवाजी ने अनेक साहसी और योग्य मराठा सरदारों को एकत्रित कर लिया था। जिसमे तुकोजी और नरायन पन्त थे । तथा इनके पिता शाहजी भोसले द्वारा 1639 ई में श्यामजी, नीलकण्ठ, सोनाजी पन्त, बालकृष्ण दीक्षित और रघुनाथ राव बल्लाल जैसे योग्य व्यक्तियों को भेजा गया ।
1643 ई0 में बीजापुर के सिंहगढ़ किले को शिवाजी द्वारा जीत लिया गया। तथा कुछ समय बाद चाकन, पुरन्दर, बारामती तोर्ना , खूपा, तिकोना, लोहगढ़, रायरी आदि किलो पर अधिकार कर लिया गया |
शिवाजी द्वारा 1648 में नीलोजी नीलकण्ठ से पुरन्दर का किला छल द्वारा विजित किया गया।
छत्रपति शिवाजी की जावली विजय:-
25 जनवरी 1656 ई. में शिवाजी और मराठा सरदार चन्द्रराव के मध्य जावली का युद्ध हुआ । इस युद्ध मे चन्द्रराव की शिवाजी द्वारा हत्या कर दी गई।
छत्रपति शिवाजी द्वारा अप्रैल 1656 ई. मे रायगढ़ को अपनी राजधानी
बनाया गया।
छत्रपति शिवाजी का पहली बार मुगलो से सामना:-
1657 ई. में मुगल शाहजादा औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया। बीजापुर के शासक आदिलशाह ने शिवाजी से सहायता मांगी।
दक्षिण में मुगलो की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए शिवाजी
ने बीजापुर की सहायता की। तथा मुगल सेना पर आक्रमण कर
परेशान किया था और जुन्नार को लूट लिया।
कालांतर में बीजापुर द्वारा मुगलों से संधि कर ली गई तब शिवाजी ने भी आक्रमण करना बंद कर दिया।
छत्रपति शिवाजी और अफजल खाँ :-
बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा मुगलों से संधि करके उनके आक्रमण के भय से मुक्त हो गया । तथा छत्रपति शिवाजी की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए तत्पर हो गया।
1659 ई. में बीजापुर राज्य ने शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए सरदार अफजल खाँ को 10,000 घुडसवार तथा तोप खाने के साथ भेजा। शिवाजी को भयभीत करने के लिए अफजल खाँ गाँव- गांव उजाड़ दिये तथा मन्दिरों को तोपो से तोड़ दिया गया।
अफजल खां द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में युद्ध करना कठिन देखकर कूटनीति से विजय करने के उद्देश्य से अपने दूत कृष्णा जी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा और मिलने की इच्छा प्रकट की |
कृष्णाजी भास्कर ने शिवाजी को यह संदेश दिया कि वह बीजापुर का अधिपत्य स्वीकार कर ले तो आदिलशाह क्षमा के साथ साथ उसका राज्य भी बना रहेगा।
कृष्णा जी भास्कर एक हिन्दू था । शिवाजी द्वारा उसे धर्म की दुहाई देकर उसके मन की बात जानने का प्रयास किया। जिसके फलस्वरूप अफजल खा की नियत कुछ ठीक नहीं का अनुमान शिवाजी को हो गया था।
प्रतापगढ़ के निकट अफजल खाँ और शिवाजी की मुलाकात होना निश्चित हुआ। दोनो केवल दो – दो अंगरक्षकों के साथ आयेगें। तथा शिवाजी को बिना अस्त्र शस्त्र आना था। लेकिन शिवाजी द्वारा बघनख, लोहे की टोपी,कटार आदि छुपाकर धारण की गई।
अफजल खाँ के साथ प्रख्यात तलवार बाज सैयद बाँदा था। शिवाजी का दूत गोपीनाथ था ।
2 नवम्बर 1659 ई. प्रतापगढ़ के वार नामक स्थान पर अफजल खाँ द्वारा शिवाजी पर तलवार से प्रहार किया लेकिन बड़ी चालाकी से शिवाजी द्वारा अफजल खाँ की हत्या कर दी गई।
,
अफजल खाँ की हत्या के बाद उसके रक्षक सैयद बाँदा ने प्रहार किया लेकिन जीवमहल शिवाजी के रक्षक द्वारा उसका हाथ काट दिया गया।
मराठा सेना द्वारा बीजापुर की सेना पर भयंकर आक्रमण किया और उसे परास्त किया।
छत्रपति शिवाजी और शाइस्ता खाँ :-
1660 ई मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा शाइस्ता खाँ को दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसने बीजापुर से मिलकर शिवाजी को समाप्त करने की योजना बनाई । वह कुछ हद तक सफल रहे क्योंकि शिवाजी को पूना, चाकन और कल्याण से हाथ धोना पड़ा।
15 अप्रैल 1663 ई. शिवाजी 400 सैनिको के साथ बारात के रूप में पूना मे घुस गए तथा अचानक आक्रमण कर दिया इस आक्रमण से भयभीत होकर शाइस्ताखां भाग खड़ा हुआ। लेकिन शिवाजी द्वारा इसका एक अंगूठा काटने में सफलता मिली।
छत्रपति शिवाजी और राजा जयसिंह :-
1665 ई में औरंगजेब ने राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा । राजा जयसिंह एक योग्यतम् सेनापति और कूटनीतिज्ञ था। वह फारसी, उर्दू, तुर्की, राजस्थानी भाषा का ज्ञाता था।
शाहजहाँ के शासन काल में राजा जयसिंह द्वारा सैकड़ो युद्ध में भाग लिया गया। तथा उनमें जीत हासिल की।
शिवाजी के विरुद्ध अभियान के समय राजा जयसिंह की उम्र 60 वर्ष होते हुए भी उसे इस अभियान की बागड़ोर सौपी गई।
जयसिंह द्वारा कूटनीति के द्वारा , बीजापुर, मराठा सरदार (जो सरदार शिवाजी से नफरत रखते थे) यूरोपीय शक्तियों को शिवाजी के पक्ष मे जाने से रोकने में सफलता प्राप्त की।
जयसिंह द्वारा कूटनीतिक मजबूती के साथ आक्रमण किया गया। वज्रगढ़ पर विजय के बाद शिवाजी को पुरन्दर के किले में घेर लिया। मजबूरन शिवाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ा ।
छत्रपति शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य पुरन्दर की संधि :-
शिवाजी बिना किसी शर्त के राजा जयसिंह से मिलने गए। और दोनों के मध्य 22 जून 1665 ई. मे पुरंदर की संधि की गई |
इस संधि मे 23 किले और 4 लाख हूण की वार्षिक आय की भूमि शिवाजी द्वारा मुगलो को देना स्वीकार किया गया।
शिवाजी के पास अब 12 किले और एक लाख हूण की वार्षिक आय की जमीन रह गयी 1
इस संधि में शिवाजी ने स्वयं न जाकर अपने पुत्र शम्भाजी को लगभग 5000 घुडसवारों के साथ मुगलो की सेवा मे भेजना स्वीकार किया।
शिवाजी द्वारा मुगलो का अधिपत्य स्वीकार कर लिया और बीजापुर के विरुद्ध मुगलो को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया।
कुछ समय पश्चात शिवाजी द्वारा एक शर्त के अनुसार, कोंकण और बालाघाट की भूमि के बदले मुगलो को 13 वर्षो मे 40 लाख
हूण देना स्वीकार किया।
1666 में शिवाजी मुगल प्रदेश की सुबेदारी और सीढ़ियों से जंजीरा
का टापू प्राप्त हो जाने के लालच में औरंगजेब से मिलने आगरा जाना स्वीकार किया।
शिवाजी और औरंगजेब की मुलाकात कराने हेतु जयसिंह ने अपने पुत्र रामसिंह को नियुक्त किया।
9 मई 1666 ई० को शिवाजी अपने पुत्र शम्भाजी और 4000
मराठा सैनिकों के साथ आगरा पहुंचें।
औरंगजेब द्वारा शिवाजी के साथ उचित व्यवहार नही किया गया। जिससे शिवाजी ने अपना अपमान समझा और बीमारी का बहाना करके बादशाह से मिलने से इनकार कर दिया।
शिवाजी को रामसिंह की देख रेख मे जयपुर भवन में नजरबन्द कर लिया गया।
छत्रपति शिवाजी द्वारा अपने सौतेले भाई हीरो जी को अपना कड़ा पहनाकर अपने विस्तर पर लिटाकर स्वयं व पुत्र शम्भाजी मिठाई के खाली टोकरों में बैठकर भागने में सफल हुए ।
1670 ई. में शिवाजी ने मुगलों से पुनः युद्ध करना आरम्भ कर दिया। कुछ ही वर्षो में मुगलों और बीजापुर से अनेक किले तथा भू-भाग जीतने मे सफलता प्राप्त की।
नानाजी द्वारा कोंगना के किले को जीत लिया गया जिसे शिवाजी द्वारा सिंहगढ़ का नाम दिया।
13 अक्टूबर 1670 को दिलेर खाँ और शाहजादा मुअज्जम के झगड़े का लाभ उठाकर शिवाजी ने सूरत का बन्दरगाह दोबारा लूट लिया।
शिवाजी द्वारा अब तक पुरंदर , कल्याण, माहुली, सलहेर, मुल्हेर, पन्हाला, पार्ली और सतारा आदि किलो को जीत के साथ-साथ जवाहरनगर और रामनगर को जीत लिया गया।
16 जून 1674 ई. में काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक कराया गया। छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को राजधानी बनाया।
राज्याभिषेक के 12 दिन पश्चात शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु हो गई।
शिवाजी के भाई व्यंकोजी ने शिवाजी का अधिपत्य स्वीकार कर शासन करते रहें।
वर्षो युद्ध करके शिवाजी द्वारा कोंकण प्रदेश पर अधिकार कर लिया गया लेकिन जंजीरा के टापू और सीदियों को अपने अधिकार मे लेने में असफल रहे।
14 अप्रैल 1680 ई. को 53 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी की बीमारी के
कारण मृत्यु हो गई |
और पढ़े :- तहकीक-ए-हिंद(Tahqiq-I-Hind)|ताज उल मासिर(Taj Ul Maasir)

 और पढ़े :-
और पढ़े :-